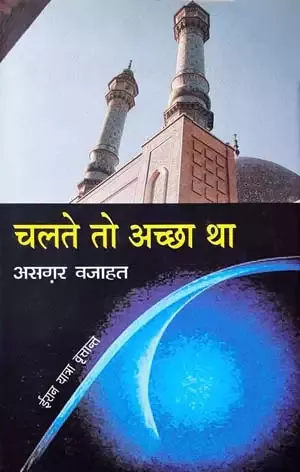|
यात्रा वृत्तांत >> चलते तो अच्छा था चलते तो अच्छा थाअसगर वजाहत
|
105 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है पुस्तक चलते तो अच्छा था ...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
चलते तो अच्छा था ईरान और आजरबाईजान के यात्रा-संस्मरण हैं। असग़र वजाहत
ने केवल इन देशों की यात्रा ही नहीं की बल्कि उनके समाज, संस्कृति और
इतिहास को समझने का भी प्रयास किया है। उन्हें इस यात्रा के दौरान विभिन्न
प्रकार के रोचक अनुभव हुए हैं। उन्हें आजरबाईजान में एक प्राचीन हिन्दू
अग्नि मिला। कोहेखाफ़ की परियों की तलाश में भी भटके और तबरेज़में एक ठग
द्वारा ठगे भी गए।
यात्राओं का आनंद और स्वयं देखने तथा खोजने का सन्तोष चलते तो अच्छा था में जगह-जगह देखा जा सकता है। असग़र वजाहत ने ये यात्राएँ साधारण ढंग से एक आदमी के रूप में की हैं जिसके परिणाम-स्वरूप वे उन लोगों से मिल पाए हैं, जिनसे अन्यथा मिल पाना कठिन है।
भारत, ईरान तथा मध्य एशिया के बीच प्राचीन काल से लेकर मध्य युग तक बड़े प्रगाढ़ सम्बन्ध रहे हैं। इसके चलते आज भी ईरान और मध्य एशिया में भारत की बड़ी मोहक छवि बनी हुई है। लेकिन 19वीं और 20वीं शताब्दी में अपने पड़ोसी देशोंके साथ भारत का रिश्ता शिथिल पड़ गया था। आज के परिदृश्य में यह ज़रूरी है कि पड़ोस में उपलब्ध सम्भावनाओं पर ध्यान दिया जाए।
चलते तो अच्छा था यात्रा-संस्मरण के बहाने हमें कुछ गहरे सामाजिक और राजनीतिक सवालों पर सोचने के लिए भी मजबूर करता है।
यात्राओं का आनंद और स्वयं देखने तथा खोजने का सन्तोष चलते तो अच्छा था में जगह-जगह देखा जा सकता है। असग़र वजाहत ने ये यात्राएँ साधारण ढंग से एक आदमी के रूप में की हैं जिसके परिणाम-स्वरूप वे उन लोगों से मिल पाए हैं, जिनसे अन्यथा मिल पाना कठिन है।
भारत, ईरान तथा मध्य एशिया के बीच प्राचीन काल से लेकर मध्य युग तक बड़े प्रगाढ़ सम्बन्ध रहे हैं। इसके चलते आज भी ईरान और मध्य एशिया में भारत की बड़ी मोहक छवि बनी हुई है। लेकिन 19वीं और 20वीं शताब्दी में अपने पड़ोसी देशोंके साथ भारत का रिश्ता शिथिल पड़ गया था। आज के परिदृश्य में यह ज़रूरी है कि पड़ोस में उपलब्ध सम्भावनाओं पर ध्यान दिया जाए।
चलते तो अच्छा था यात्रा-संस्मरण के बहाने हमें कुछ गहरे सामाजिक और राजनीतिक सवालों पर सोचने के लिए भी मजबूर करता है।
मिट्टी का प्याला
दोनों तरफ सूखे, निर्जीव, ग़ैर आबाद पहाड़ थे जिन पर लगी घास तक जल चुकी
थी। सड़क इन्हीं पहाड़ों के बीच बल खाती गुज़र रही थी। रास्ता वही था
जिससे मै इस्फ़हान से होता शीराज़ पहुँचा था और अब शीराज से साठ
किलोमीटर दूर ‘पारसी-पोलास’ यानी ’तख़्ते
जमशैद’
देखने जा रहा था. शीराज़ मे पता लगा था कि ‘तख़्ते
जमशैद’ तक
‘सवारी’ टैक्सियाँ चलती हैं। ईरान में
‘सवारी’ का
मतलब वे टैक्सियाँ होती हैं जिन पर मुसाफिर अपना-अपना किराया
देकर
सफर करते हैं। ये सस्ती होती हैं। ‘तख़्ते जमशैद’ तक
जाने के
लिए शीराज के बस अड्डे पर ‘सवारी’ की तलाश में आया था
लेकिन
टैक्सीवाले ने मर्जी के ख़िलाफ़ मुझे एक टैक्सी में ठूँसा और टैक्सी चल
दी। मेरे खयाल से मुझे पाँच हज़ार रियाल देने थे और इस टैक्सी में मेरे
अलावा चार और लोगों को भी होना चाहिए था लेकिन मैं अकेला था और ज़ाहिर था
कि दूसरे चार लोगों का किराया मुझसे ही वसूल किया जाना था।
वीरान
पहाड़ों पर करीब सवा घंटे चलने के बाद टैक्सी ड्राइवर ने
‘तख़्ते
जमशैद’ की पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी। सामने दूर तक फैले
खँडहरों में ऊँचे-ऊँचे खम्भे ही नुमाया थे।
बताया जाता है कि ईसा से सात सौ साल पहले ईरान के एक जनसमूह ने जो अपने को आर्य कहता था, एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था। यह पूर्व में सिंध नदी से लेकर ईरान की खाड़ी तक फैला हुआ था। इतिहास में इस साम्राज्य को ‘हख़ामनश’ के नाम से याद किया जाता है। अंग्रेजी में इसे ‘अकामीडियन’ साम्राज्य कहते हैं। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि यह अपने समय का ही नहीं बल्कि हमारे समय में भी बड़े महत्त्व का साम्राज्य माना जाएगा।
इस साम्राज्य के एक महान शासक दारुलस प्रथम (549 जन्म-485 मृत्यु ई. पू.) ने विश्व में पहला मानव अधिकार दस्तावेज जारी किया था जो आज भी इतना महत्त्वपूर्ण है कि 1971 में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने उसका अनुवाद विश्व की लगभग सभी भाषाओं में कराया और बाँटा था। यह दस्तावेज मिट्टी के बेलन जैसे आकार के पात्र पर खोदा गया था और उसे पकाया गया था ताकि सुरक्षित रहे। दारुस ने बाबुल की विजय के बाद इसे जारी किया था। कहा जाता है कि यह मानव अधिकार सुरक्षा दस्तावेदज़ फ्रांस की क्रांति (1789-1799) में जारी किए गए मानव अधिकार मैनेफैस्टों से भी ज्यादा प्रगतिशील है। घोषणापत्र के कुछ अंश इस प्रकार हैं, ‘‘....अब मैं अहुर मज़्द (Ahura Mazda) (अग्निपूजकों के सबसे बड़े देवता) की मदद से ईरान, बाबुल और चारों दिशाओं में फैले राज्यों का मुकुट अपने सिर पर रखते हुए यह घोषणा करता हूँ कि मैं अपने साम्राज्य के सभी धर्मों, परम्पराओं और आचार-व्यवहारों का आदर करूँगा और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मेरे गवर्नर और उनके मातहत अधिकारी भी ऐसा करते रहेंगे। मैं अपनी बादशाहत किसी देश (राज्य) पर लादूंगा (आरोपित) नहीं। इसे स्वीकार करने के लिए सभी स्वतन्त्र हैं और अगर कोई इसे अस्वीकार करता है तो मैं उससे कभी युद्ध नहीं करूँगा। जब तक मैं ईरान, बाबुल और चारों दिशाओं में फैले राज्यों का सम्राट हूँ तब तक मैं किसी को किसी का शोषण नहीं करने दूँगा और अगर यह होता है तो मैं निश्चित शोषित का पक्ष लूँगा और अपराधी को दण्डित करूँगा। जब तक मैं सम्राट हूँ तब तक बिना पैसा लिए-दिए या उचित भुगतान किए बिना कोई किसी की चल-अचल सम्पत्ति पर अधिकार न कर सकेगा।
जब तक मैं जालित हूँ तब तक बेगार और बलात काम लिए जाने का विरोध करता रहूँगा। आज मैं यह घोषणा करता हूँ कि हर आदमी अपना धर्म चुनने के लिए आजाद है। लोग कहीं भी रहने के लिए स्वतन्त्र हैं और वे कोई भी काम कर सकतें हैं जब तक कि उससे दूसरों के अधिकार खंडित न होते हों....किसी को उसके रिश्तेदारों के लिए सज़ा नहीं दी जाएगी। मैं गुलामी (दासप्रथा) को प्रतिबन्धित करता हूँ और मेरे साम्राज्य के गवर्नरों तथा उनके अधिकारियों की ज़िम्मेदारी है आदमी औरतों को गुलाम की तरह बेचने-खरीदने को अपने क्षेत्र में समाप्त करें...गुलामी को पूरे संसार से समाप्त हो जाना चाहिए...मैं अहुर मज़्द से कामना करता हूँ कि साम्राज्य के प्रति मुझे अपने आश्वासनों को पूरा करने में सफलता दे।’’
ईसा से पाँच सौ साल पहले दारुस महान ने अपने राज्य का आधार फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेन्स (गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था) बनाया था। राज्यों को अधिकार दिए गए थे और केन्द्र की नीतियाँ उदार तथा जनहित में थीं। साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत व्पापार कर था जिसे बढ़ाने के साथ-साथ व्यापारियों की सुरक्षा पर ध्यान देता था। दारुस ने अपने साम्राज्य के दो कोने को जोड़नेवाले एक ढाई हज़ार मील लम्बे राजमार्ग का निर्माण भी कराया था। इतिहासकार कहते हैं कि पूरे साम्राज्य में डाक की व्यवस्था इतनी उत्तम थी कि एक कोने से दूसरे कोने तक डाक पन्द्रह दिनों में पहुँच जाती थी।
शताब्दियों तक दारुस महान की राजधानी ‘तख़्ते जमशैद’ पत्थरों, मिट्टी, धील और उपेक्षा के पहाड़ों के नीचे दबी पड़ी रही यह इलाक़ा ‘कोहे रहमत’ के नाम से जाना जाता है। रहमत का मतलब ईश्वरीय कृपा है। 1931-1934 के बीच यहाँ अमेरिकी विश्वविद्यालयों के पुरातत्व विभागों ने खुदाई का एक व्यापक अभियान चलाया था और दारुस की राजधानी के अवशेष सामने आए थे।
ईरानी सरकार जो प्रायः पर्यटन के प्रति उदासीन है ‘तख़्ते जमशैद’ की उपेक्षा नहीं कर सकी है। यहाँ पर्यटन विभाग के कार्यालय और पर्यटकों के लिए अन्य सुविधाएँ मौजूद हैं। यह अब ईरान का ही नहीं बल्कि विश्व का एक महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन गया है।
‘तख़्ते जमशैद’ आने से पहले कहीं पढ़ा था और लोगों ने बताया भी कि खंडहरों को देखकर यह कल्पना करनी चाहिए कि यह इमारत कितनी विशाल रही होगी। विस्तार का अन्दाजा तो दूर से हो जाता है। कोहे रहमत के नीचे ऊँचे खम्भों तक लम्बा सिलसिला और सामने के पहाड़ों को काटकर तराशी गई मूर्तियाँ तथा गुफाएँ नज़र आने लगते हैं।
मुख्य इमारत तक जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया तो ऊँचे-ऊँचे पत्थर के खम्भे नज़र आए। यह गारुस का दरबार हॉल था। इन खम्भों पर इमारत की कल्पना करते हुए मैंने इसकी तुलना लाल किले के दीवाने आम से की तो दीवाने आम बच्चों का खेल लगा यहाँ के दीवाने आम के खम्भों की ऊँचाई लाल किलेवाले खम्भों से कम से कम तीन गुनी है। लम्बाई और चौड़ाई में भी दारुस का दीवाने आम शाहजहाँ के दीवाने आम से छह-सात गुना बड़ा होगा। आश्चर्य यह होता है कि इतने बड़े दीवाने आम में हज़ारों लोगों तक सम्राट या अन्य अधिकारियों की आवाज़ें कैसे पहुँचती होंगी और व्यवस्था कैसे बनाई जाती होगी।
दारुस ने ‘पारसी पोलिस’ यानी ‘तख़्ते जमशैद’ का निर्माण 518 ई. पू के आसपास शुरू किया था और सौ साल बाद यह निर्माण कार्य पूरा हुआ था। दारुस ने ‘तख़्ते जमशैद’ की परिकल्पना केवल एक महल या किले के रूप में नहीं की थी। वह ऐसे-ऐसे विशाल स्थान का निर्माण करना चाहता था जिसका कोई दूसरी मिसाल न हो। वह चाहता था कि साम्राज्य की शक्ति, वैभव, सम्पन्नता, बुद्धिमत्ता और सौन्दर्यप्रियता को दर्शानेवाली इमारतों का एक समूह बनाया जाए तो अद्वितीय हो। दारुस के पुत्र जेरजेस (518-465 ई.पू.) की शपथ—‘‘मैं उस काम को पूरा करूँगा जो मेरे पिता ने शुरू किया था’’ दीवार पर अंकित है।
ऊपर तेज सूरज चमक रहा था जिसकी रोशनी में कई किलोमीटर फैले खंडहर अतीत की रहस्यमयी कहानियाँ सुना रहे थे। पर्यटक यहाँ काफी थे लेकिन क्षेत्र इतना बड़ा था कि बस खेत में कुछ दाने की तरह छिटके ही दिखाई पड़ रहे थे कि उन पर नज़र ज़माना भी मुश्किल था। दीवने आम के पीछे दूसरी इमारतो के खंडहर थे जो दूर फैले चले गए थे और ‘कोहे रहमत’ में बनी गुफाओं से मिल गए थे। यह देखने के लिए एक दिन काफी था। दरवाज़ों पर पत्थर से काटी गई देवताओं की मूर्तियाँ, कहीं सिपाहियों की आकृतियाँ और पहाड़ों पर युद्ध के दृश्य साम्राज्य और सम्राटों की जिन्दगी के जीवित दस्तावेज लगते थे।
‘तख़्ते जमशैद’ से कुछ किलोमीटर दूर नक्शे रुस्तम’ है। रुस्तम भी एक पौराणिक चरित्र है जिसने फिरदौसी के ‘शाहनामें में अमर कर दिया है। उसने कल्पना-कला और मार्मिकता की ऊँचाइयाँ को छू लिया है। बुनियादी तौर पर योद्धा होने के साथ-साथ वह प्रेमी भी है, दाता भी है, संवेदनशील पिता भी है और एक त्रासदी का नायक भी है। ‘नक्शे रुस्तम’ पहाड़ पर एक ऐसा जगह है जो समतल है। कहा जाता है कि रुस्तम यहाँ नाचा था इस कारण पहाड़ का यह हिस्सा समतल हो गया। ‘नक्शे रुस्तम’ पहाड़ी को सम्राटों की गैलरी भी कहा जाए तो गलत न होगा। यहाँ ‘हख़ामनश’ साम्राज्य ही नहीं बल्कि पूर्व और परवर्ती साम्राज्य जैसे सासानी साम्राज्य के सम्राटों ने भी अपनी विजयों से संबंधित चित्र पत्थर पर अंकित कराए हैं। इस स्थान पर सम्राटों के मक़बरे बनाने तथा उन पर इतिहास अंकित करने की भी परम्परा रही है। यहीं पत्थर पर तराश कर बनाए गए चित्रों में सामानी सम्राट शापुर प्रथम (241-272 ई.पू.) का वह प्रसिद्ध चित्र भी है जिसमें ईरानियों से पराजित रोम का सम्राट वैरियन घुटने टेके शापुर प्रथम के सामने बैठा है और शापुर घोड़े पर सवार है। कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि ईरान सम्राट शापुर प्रथम ने पराजित रोम के सम्राट को अपने दरबार में घुटने के बल टेकर (260 ई.पू.) आने के लिए बाध्य किया था और इस घटना का आतंक शताब्दियों क़ायम रहा था।
कोई गाइट किसी पर्यटक ग्रुप को एक दीवार दिखाकर बता रहा था कि कभी यह दीवार इतनी चमकीली हुआ करती थी कि लोग इसमें अपनी शकल देख लिया करते थे। इस तरह की न जाने कितनी गाथाएँ यहाँ से जुड़ी हैं। कहते हैं कि किसी पौराणिक सम्राट जमशैद की भी यही राजधानी होती थी उसके पास एक दैवी प्याला था जो ‘जामे जमशैद’ के नाम से मशहूर है। जमशैद का जिक्र फिरदैसी ने ‘शाहनामा’ में भी किया है। प्याले में वह पूरे संसार की छवियाँ तथा भविष्य और भूत को देख सकता था।
बताया जाता है कि ईसा से सात सौ साल पहले ईरान के एक जनसमूह ने जो अपने को आर्य कहता था, एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था। यह पूर्व में सिंध नदी से लेकर ईरान की खाड़ी तक फैला हुआ था। इतिहास में इस साम्राज्य को ‘हख़ामनश’ के नाम से याद किया जाता है। अंग्रेजी में इसे ‘अकामीडियन’ साम्राज्य कहते हैं। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि यह अपने समय का ही नहीं बल्कि हमारे समय में भी बड़े महत्त्व का साम्राज्य माना जाएगा।
इस साम्राज्य के एक महान शासक दारुलस प्रथम (549 जन्म-485 मृत्यु ई. पू.) ने विश्व में पहला मानव अधिकार दस्तावेज जारी किया था जो आज भी इतना महत्त्वपूर्ण है कि 1971 में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने उसका अनुवाद विश्व की लगभग सभी भाषाओं में कराया और बाँटा था। यह दस्तावेज मिट्टी के बेलन जैसे आकार के पात्र पर खोदा गया था और उसे पकाया गया था ताकि सुरक्षित रहे। दारुस ने बाबुल की विजय के बाद इसे जारी किया था। कहा जाता है कि यह मानव अधिकार सुरक्षा दस्तावेदज़ फ्रांस की क्रांति (1789-1799) में जारी किए गए मानव अधिकार मैनेफैस्टों से भी ज्यादा प्रगतिशील है। घोषणापत्र के कुछ अंश इस प्रकार हैं, ‘‘....अब मैं अहुर मज़्द (Ahura Mazda) (अग्निपूजकों के सबसे बड़े देवता) की मदद से ईरान, बाबुल और चारों दिशाओं में फैले राज्यों का मुकुट अपने सिर पर रखते हुए यह घोषणा करता हूँ कि मैं अपने साम्राज्य के सभी धर्मों, परम्पराओं और आचार-व्यवहारों का आदर करूँगा और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मेरे गवर्नर और उनके मातहत अधिकारी भी ऐसा करते रहेंगे। मैं अपनी बादशाहत किसी देश (राज्य) पर लादूंगा (आरोपित) नहीं। इसे स्वीकार करने के लिए सभी स्वतन्त्र हैं और अगर कोई इसे अस्वीकार करता है तो मैं उससे कभी युद्ध नहीं करूँगा। जब तक मैं ईरान, बाबुल और चारों दिशाओं में फैले राज्यों का सम्राट हूँ तब तक मैं किसी को किसी का शोषण नहीं करने दूँगा और अगर यह होता है तो मैं निश्चित शोषित का पक्ष लूँगा और अपराधी को दण्डित करूँगा। जब तक मैं सम्राट हूँ तब तक बिना पैसा लिए-दिए या उचित भुगतान किए बिना कोई किसी की चल-अचल सम्पत्ति पर अधिकार न कर सकेगा।
जब तक मैं जालित हूँ तब तक बेगार और बलात काम लिए जाने का विरोध करता रहूँगा। आज मैं यह घोषणा करता हूँ कि हर आदमी अपना धर्म चुनने के लिए आजाद है। लोग कहीं भी रहने के लिए स्वतन्त्र हैं और वे कोई भी काम कर सकतें हैं जब तक कि उससे दूसरों के अधिकार खंडित न होते हों....किसी को उसके रिश्तेदारों के लिए सज़ा नहीं दी जाएगी। मैं गुलामी (दासप्रथा) को प्रतिबन्धित करता हूँ और मेरे साम्राज्य के गवर्नरों तथा उनके अधिकारियों की ज़िम्मेदारी है आदमी औरतों को गुलाम की तरह बेचने-खरीदने को अपने क्षेत्र में समाप्त करें...गुलामी को पूरे संसार से समाप्त हो जाना चाहिए...मैं अहुर मज़्द से कामना करता हूँ कि साम्राज्य के प्रति मुझे अपने आश्वासनों को पूरा करने में सफलता दे।’’
ईसा से पाँच सौ साल पहले दारुस महान ने अपने राज्य का आधार फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेन्स (गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था) बनाया था। राज्यों को अधिकार दिए गए थे और केन्द्र की नीतियाँ उदार तथा जनहित में थीं। साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत व्पापार कर था जिसे बढ़ाने के साथ-साथ व्यापारियों की सुरक्षा पर ध्यान देता था। दारुस ने अपने साम्राज्य के दो कोने को जोड़नेवाले एक ढाई हज़ार मील लम्बे राजमार्ग का निर्माण भी कराया था। इतिहासकार कहते हैं कि पूरे साम्राज्य में डाक की व्यवस्था इतनी उत्तम थी कि एक कोने से दूसरे कोने तक डाक पन्द्रह दिनों में पहुँच जाती थी।
शताब्दियों तक दारुस महान की राजधानी ‘तख़्ते जमशैद’ पत्थरों, मिट्टी, धील और उपेक्षा के पहाड़ों के नीचे दबी पड़ी रही यह इलाक़ा ‘कोहे रहमत’ के नाम से जाना जाता है। रहमत का मतलब ईश्वरीय कृपा है। 1931-1934 के बीच यहाँ अमेरिकी विश्वविद्यालयों के पुरातत्व विभागों ने खुदाई का एक व्यापक अभियान चलाया था और दारुस की राजधानी के अवशेष सामने आए थे।
ईरानी सरकार जो प्रायः पर्यटन के प्रति उदासीन है ‘तख़्ते जमशैद’ की उपेक्षा नहीं कर सकी है। यहाँ पर्यटन विभाग के कार्यालय और पर्यटकों के लिए अन्य सुविधाएँ मौजूद हैं। यह अब ईरान का ही नहीं बल्कि विश्व का एक महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन गया है।
‘तख़्ते जमशैद’ आने से पहले कहीं पढ़ा था और लोगों ने बताया भी कि खंडहरों को देखकर यह कल्पना करनी चाहिए कि यह इमारत कितनी विशाल रही होगी। विस्तार का अन्दाजा तो दूर से हो जाता है। कोहे रहमत के नीचे ऊँचे खम्भों तक लम्बा सिलसिला और सामने के पहाड़ों को काटकर तराशी गई मूर्तियाँ तथा गुफाएँ नज़र आने लगते हैं।
मुख्य इमारत तक जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया तो ऊँचे-ऊँचे पत्थर के खम्भे नज़र आए। यह गारुस का दरबार हॉल था। इन खम्भों पर इमारत की कल्पना करते हुए मैंने इसकी तुलना लाल किले के दीवाने आम से की तो दीवाने आम बच्चों का खेल लगा यहाँ के दीवाने आम के खम्भों की ऊँचाई लाल किलेवाले खम्भों से कम से कम तीन गुनी है। लम्बाई और चौड़ाई में भी दारुस का दीवाने आम शाहजहाँ के दीवाने आम से छह-सात गुना बड़ा होगा। आश्चर्य यह होता है कि इतने बड़े दीवाने आम में हज़ारों लोगों तक सम्राट या अन्य अधिकारियों की आवाज़ें कैसे पहुँचती होंगी और व्यवस्था कैसे बनाई जाती होगी।
दारुस ने ‘पारसी पोलिस’ यानी ‘तख़्ते जमशैद’ का निर्माण 518 ई. पू के आसपास शुरू किया था और सौ साल बाद यह निर्माण कार्य पूरा हुआ था। दारुस ने ‘तख़्ते जमशैद’ की परिकल्पना केवल एक महल या किले के रूप में नहीं की थी। वह ऐसे-ऐसे विशाल स्थान का निर्माण करना चाहता था जिसका कोई दूसरी मिसाल न हो। वह चाहता था कि साम्राज्य की शक्ति, वैभव, सम्पन्नता, बुद्धिमत्ता और सौन्दर्यप्रियता को दर्शानेवाली इमारतों का एक समूह बनाया जाए तो अद्वितीय हो। दारुस के पुत्र जेरजेस (518-465 ई.पू.) की शपथ—‘‘मैं उस काम को पूरा करूँगा जो मेरे पिता ने शुरू किया था’’ दीवार पर अंकित है।
ऊपर तेज सूरज चमक रहा था जिसकी रोशनी में कई किलोमीटर फैले खंडहर अतीत की रहस्यमयी कहानियाँ सुना रहे थे। पर्यटक यहाँ काफी थे लेकिन क्षेत्र इतना बड़ा था कि बस खेत में कुछ दाने की तरह छिटके ही दिखाई पड़ रहे थे कि उन पर नज़र ज़माना भी मुश्किल था। दीवने आम के पीछे दूसरी इमारतो के खंडहर थे जो दूर फैले चले गए थे और ‘कोहे रहमत’ में बनी गुफाओं से मिल गए थे। यह देखने के लिए एक दिन काफी था। दरवाज़ों पर पत्थर से काटी गई देवताओं की मूर्तियाँ, कहीं सिपाहियों की आकृतियाँ और पहाड़ों पर युद्ध के दृश्य साम्राज्य और सम्राटों की जिन्दगी के जीवित दस्तावेज लगते थे।
‘तख़्ते जमशैद’ से कुछ किलोमीटर दूर नक्शे रुस्तम’ है। रुस्तम भी एक पौराणिक चरित्र है जिसने फिरदौसी के ‘शाहनामें में अमर कर दिया है। उसने कल्पना-कला और मार्मिकता की ऊँचाइयाँ को छू लिया है। बुनियादी तौर पर योद्धा होने के साथ-साथ वह प्रेमी भी है, दाता भी है, संवेदनशील पिता भी है और एक त्रासदी का नायक भी है। ‘नक्शे रुस्तम’ पहाड़ पर एक ऐसा जगह है जो समतल है। कहा जाता है कि रुस्तम यहाँ नाचा था इस कारण पहाड़ का यह हिस्सा समतल हो गया। ‘नक्शे रुस्तम’ पहाड़ी को सम्राटों की गैलरी भी कहा जाए तो गलत न होगा। यहाँ ‘हख़ामनश’ साम्राज्य ही नहीं बल्कि पूर्व और परवर्ती साम्राज्य जैसे सासानी साम्राज्य के सम्राटों ने भी अपनी विजयों से संबंधित चित्र पत्थर पर अंकित कराए हैं। इस स्थान पर सम्राटों के मक़बरे बनाने तथा उन पर इतिहास अंकित करने की भी परम्परा रही है। यहीं पत्थर पर तराश कर बनाए गए चित्रों में सामानी सम्राट शापुर प्रथम (241-272 ई.पू.) का वह प्रसिद्ध चित्र भी है जिसमें ईरानियों से पराजित रोम का सम्राट वैरियन घुटने टेके शापुर प्रथम के सामने बैठा है और शापुर घोड़े पर सवार है। कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि ईरान सम्राट शापुर प्रथम ने पराजित रोम के सम्राट को अपने दरबार में घुटने के बल टेकर (260 ई.पू.) आने के लिए बाध्य किया था और इस घटना का आतंक शताब्दियों क़ायम रहा था।
कोई गाइट किसी पर्यटक ग्रुप को एक दीवार दिखाकर बता रहा था कि कभी यह दीवार इतनी चमकीली हुआ करती थी कि लोग इसमें अपनी शकल देख लिया करते थे। इस तरह की न जाने कितनी गाथाएँ यहाँ से जुड़ी हैं। कहते हैं कि किसी पौराणिक सम्राट जमशैद की भी यही राजधानी होती थी उसके पास एक दैवी प्याला था जो ‘जामे जमशैद’ के नाम से मशहूर है। जमशैद का जिक्र फिरदैसी ने ‘शाहनामा’ में भी किया है। प्याले में वह पूरे संसार की छवियाँ तथा भविष्य और भूत को देख सकता था।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book